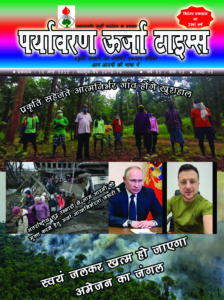वर्तमान परिदृश्य में सभ्यता के समक्ष व्याप्त प्रदूषण के विभिन्न आयामों में मूलतः जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण पर ही सर्वाधिक चर्चा होती है। किन्तु यदि गंभीरता से चिंतन किया जावे तो हमारे परिवेशीय आकाश में बढ़ते प्रकाश की मात्रा, तीव्रता और अवधि भी तो एक प्रकार का प्रदूषण ही माना जा सकता है? प्रकृति ने पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव-जंतु एवं वनस्पतियों का सृजन किया, जिसमें बहुत सारे वनों में विचरण करने वाले पशु-पक्षियों को रात्रीय अंधकार में जीने का न केवल अभ्यास था, अपितु उनके स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए वह आवश्यक था और है भी। किन्तु वर्तमान सभ्यता के प्रगति पथ ने इनके वनीय वातावरण की रात्रि की नीरवता एवं अंधकार को बहुत गंभीर रूप से क्षत-विक्षत किया है।
परिणामस्वरूप, अनेकों पशु-पक्षी अपने प्राकृतिक प्रजनन प्रणाली के पथ से विमुख हो चुके हैं या होते जा रहे हैं। जिसकी परिणिति यह है कि उनकी प्रजनन प्रक्रिया बाधित हो रही है। तदैव, उनकी संततियों (च्तवहमदल) की संख्या कम हो रही है। यदि नहीं हो भी रही है तो उनमें अनेकों प्रकार की ऐसी विकृतियां हैं कि वे सुरक्षित या स्वस्थ ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। परिणामस्वरूप भी अनेकों वन्य जीव प्रजातियों का लोप हो रहा है।
जिस प्रकार से अनेकों प्राणियों में रात्रीय अंधकार की आवश्यकता उनके सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है, तो ऐसा लगता है कि वनस्पतियों में भी रात्रि अंधकार (छपहीज क्ंतादमेे) का महत्व अवश्य होता होगा। यद्यपि इस विषय पर कोई अनुसंधन अभी तक नहीं किया गया है, किन्तु प्रकाश संलेश्षण करने वाली पर्णीय कोशिकाओं को भी तो प्रतिदिन कुछ समय प्रकाश विहीन अवस्था में विश्राम की अपेक्षा तो होती होगी?
यह एक विडंबना ही है कि अभी तक मनुष्य एवं हमारी वैज्ञानिक सभ्यता के लोग पौधों में पत्तों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन अवशोषित कर ऊर्जा संचय को ही सबसे बड़ा उत्पादन का पैमाना मानते हैं, किन्तु क्या पौधों के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे की अवधि में कुछ 10-12 घंटों का अंधकार दिन भर संचित किए कार्बन को कार्बोहाइड्रेट से आगे की महत्वपूर्ण जीवन पोषीय संरचनाओं (यथा एल्केलायड, विटामिन, प्रोटीन आदि) की श्रृंखला में परिवर्तन करने हेतु अपेक्षित नहीं होता होगा?
अस्तु वनों में बढ़ते प्रकाश प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर चिंता अभी तक कम ही की गई है। किन्तु वरिष्ठ वन वैज्ञानिकों में से कुछेक को निश्चित रूप से प्रकाश प्रदूषण का यह आयाम भी चिंतनीय लगता है। आज की स्थिति यह है कि अनेकों घनघोर वनों में कोयला, लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के दोहन के लिए रात में भी तेज कृत्रिम विद्युत ऊर्जा जनित प्रकाश के प्रकाश में उत्खनन कार्य जारी रहता है, तो अनेकों हाईवे तथा एक्सप्रेसवे में चलने वाले वाहनों से भी तेज प्रकाश वनों में फैलता है। इसके अतिरिक्त इन गतिविधियों से ध्वनि का भी स्तर उच्च होता है। एक युग था, जब गांवों में अमावस्या के दिन आसमान में तारों की जगमगाहट मन को मोह लेती थी। सयाने लोग अपने पोते-पोतियों, नाती-नातिनों को ध्रुव तारे से लेकर अश्विन, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, स्वाती, पुनर्वसु, सप्तर्षि आदि सैकड़ों तारों से परिचय कराते थे। उनकी पौराणिक कहानियां सुनाते थे। अंधकार भरी रात में ये तारे पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। पर आज तो शहरी क्षेत्रों में बढ़ चुके प्रकाश प्रदूषण के कारण शहरों के आकाश में तो अमावश्या में भी इन तारों के दर्शन पूरी तरह से दुर्लभ हो गए हैं और तारामंडल (Planotorium) को छोड़कर तो दिगंत में व्याप्त इन तारों की चर्चा कोई शायद ही कभी करता हो? अस्तु, चिंतन तथा अनुसंधान का विषय यह भी हो कि क्या वर्तमान सभ्यता में बढ़ते हुए प्रकाश के प्रयोग से मानव शरीर पर भी बुरा असर तो नहीं हो रहा है? घटती रोगरोधन क्षमता के अनेकों कारणों में से शायद क्या यह भी एक हो सकता है।
पर्याप्त निद्रा का अभाव जिस प्रकार से मानव के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है, मनुष्य के रोगरोधन क्षमता में गिरावट आती है, तो मधुमेह, गठिया, वात जैसे रोगों की शिकायत भी पनपती है, तो अपर्याप्त रात्रि विश्राम क्या पशुओं को प्रभावित नहीं करती होगी? जैविक विविधता के हलास के अनेकों कारणों में क्या अंधकार की पर्याप्तता का अभाव भी एक कारण हो सकता है? प्रकृति ने पृथ्वी पर जो जीवन चक्र की सुगमता के लिए व्यवस्था की थी और की है, वह अत्यंत जटिल तथा विस्मयकारी है। मनुष्य भले ही उसे समझने के लिए कितने ही प्रयास करे, पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस परम ज्ञान को पाना बहुत ही दुष्कर है।
मनुष्य के द्वारा कृत्रिम ऊर्जा उत्पन्न करने के ज्ञान और तकनीकी ने अप्राकृतिक जीवनशैली के लिए कृत्रिम ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किन्तु उसके तात्कालिक एवं दूरगामी दुष्परिणाम काफी तो समक्ष आ चुके हैं और कुछ तो समझ में भी आ रहे हैं। पर बहुत सारे दुष्परिणामों का अनुमान करना भी दूभर है।
उदाहरण के तौर पर हम पृथ्वी पर बढ़ते तापमान की गणना के अनुमान का ही मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि यह मूल्यांकन ज्यादातर हरितकारी गैसों (ळभ्ळ) के बढ़ते सांद्रण (स्तर) पर ही गणित किया गया है। किन्तु इसके समानांतर जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि पृथ्वी पर औद्योगिक सभ्यता के पूर्व और आज तक भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन किया गया है और क्या परिवर्तन अपेक्षित है, तो उसमें सबसे प्रमुख बात यह आती है कि पृथ्वी पर आच्छादित हरीतिमा का स्तर बहुत तेजी से कम हुआ है, जिसमें वन क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों एवं हरित मैदानी क्षेत्रों में आई तेज गिरावट तो स्पष्ट हैं। वहीं पृथ्वी पर भू-उपयोग में हरितिमा विहीन उपयोग यथा नगरीय बसाहट, उद्योग, अधोसंरचनाएं, खदान आदि के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। एक प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में पेड़-पौधों को समाप्त कर कांक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। इसके दुष्परिणाम स्वतः स्पष्ट हैं। हरित क्षेत्रों में कमी के कारण सौर ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन संचय में गिरावट तो आई ही है और हरित क्षेत्रों में प्रकाश के परावर्तन के कारण परिवेशीय तापमान के नियंत्रण (गिरावट) की क्षमता में भी गिरावट आई है। तो वहीं कांक्रीट के जंगलों के कारण भवनों पर पड़ने वाले सौर प्रकाश में व्याप्त विकरित ऊष्मा ऊर्जा के ताप संचय के कारण परिवेशीय तापमान में वृद्धि में भी काफी योगदान हो रहा है। इस प्रकार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि में बढ़ते भवन निर्मित क्षेत्रों का भी काफी बड़ा योगदान बढ़ रहा है।
ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा हर घर सौर ऊर्जा घर का संकल्प एक स्वागतेय संकल्प है। इसके परिणाम निश्चित रूप से पर्यावरण हितकारी तथा स्वच्छ ऊर्जा संवर्धी होंगे। समय की मांग है कि प्रत्येक नागरिक अपने घरों में यथाश्रेष्ठ संभव साधनों का उपयोग कर संपूर्ण भारत के नगरों तथा गांवों में आसमान में खुली छतों पर सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु सुविधाएं स्थापित करें। इसमें राष्ट्र को चैतरफा लाभ होगा। एक तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन में वृद्धि होगी, हर घर ऊर्जा आत्मनिर्भर होगा, स्थानीय परिवेशीय तापमान में घरों की छतों के द्वारा किए जाने वाले ताप वृद्धि योगदान में कमी आवेगी, तो पूरे देश के छतों को सौर ऊर्जा छतों में परिवर्तन करने हेतु रोजगार में भी वृद्धि होगी। देश के नागरिकों को इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण के जैसे ही जल संरक्षण के लिए प्रयास करना जरूरी है।
इस वर्ष मार्च के अंत होते-होते ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही भारत के अनेकों शहरों में भूमिगत जल लगभग समाप्त हो चुका है। हजारों ट्यूबवेल सूख चुके हैं। बंगालुरू, चेन्नई जैसे महानगरों में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गंभीर जल संकट सामने दिखाई दे रहा है। यद्यपि महानगरों में जल आपूर्ति के लिए महानगर निगमों, नगर निगमों के द्वारा जल आपूर्ति के लिए भूमिगत जल के अतिरिक्त भू-सतही जल स्रोतों से आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है, किन्तु जल संकट की तीक्ष्णता केवल मात्रात्मक आपूर्ति के अभाव तक सीमित नहीं है, अपितु ग्रीष्मकालीन उपलब्ध जल में गुणवत्तात्मक गिरावट भी चिंताजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रतिवर्ष सम्पूर्ण भारत में दूषित जल उपभोग के कारण गरीब बस्तियों में अनेकों प्रकार की महामारियां यथा हैजा, दस्त, बुखार आदि के प्रकोप के समाचार छपते रहते हैं। किंतु इन समस्याओं के समाधान हेतु जन सामान्य के द्वारा सामाजिक स्तर पर जो प्रयास किए जाने चाहिए, उनका नितांत अभाव लगता है। हमें अब यह स्वीकार करना चाहिए कि भूमिगत जल संकट या भूस्तरीय जल संकट की स्थिति नागरिकों के द्वारा वर्षा जल संधारण तथा उपभोग में जल संरक्षण के प्रति व्याप्त उपेक्षा का परिणाम भी है। यद्यपि भूमिगत जल दोहन को नियामित करने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा अनेकों नियमों को निरूपित किया गया है, किन्तु किसी भी प्रशासन के लिए यह संभव नहीं है कि भूमिगत जल दोहन के सभी स्रोतों की निरंतर निगरानी करके प्रत्येक उल्लंघनकर्ता को विधिक प्रावधानों की अवहेलना के लिए दंडित कर सके। जल संकट के आपातकाल का एक प्रमुख सामाजिक कारण जनसंख्या विस्फोट भी है। किन्तु बहुत कम ही सामाजिक संस्थान या धार्मिक संस्थान प्रकृति के सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन के लिए नागरिकों को सुशिक्षित करने हेतु तत्परता दिखाते हैं। अस्तु वर्तमान परिदृश्य में पारिस्थितिकी से संबंधित संकटमय परिस्थितियों के समाधान की पहल तो पहले सामाजिक स्तर पर जन-जागरूकता से भी करना होगा, तभी हम अपने वर्तमान पीढ़ी एवं भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित जल, वायु एवं पृथ्वी प्रदान कर सकेंगे। पृथ्वी पर व्यापक हो चुके पर्यावरणीय संकट, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण हेतु उदासीन सामाजिक पहल की स्थिति अत्यंत चिताजनक है। लोग इन समस्याओं को बहुत ही हल्के में लेते हैं, जबकि स्थिति आपातकाल सी हो चुकी है। अतः इस लेख के माध्यम से सभी सुधी पाठकों से आव्हान है कि अब केवल चिंतन और चर्चा का समय नहीं रहा। अब सबको तत्काल पर्यावरण बचाने के काम में जुट जाना जरूरी है। सभी पाठकों को ‘हिन्दू नववर्ष’ विक्रम संवत 2081 एवं ‘चैत्र नवरात्रि’ की शुभकामनाएं।
-संपादक