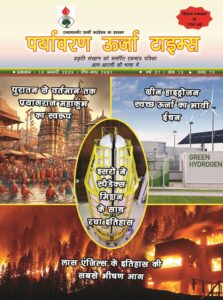हर साल सम्पूर्ण विश्व में ‘‘विश्व पर्यावरण दिवस’’ 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम ‘‘भूमि पुनस्र्थापन, मरूस्थलीकरण और सूखा लचीलापन’’ है, जिसके लिए नारा दिया गया है ‘‘हमारी भूमि हमारा भविष्य’’। भूमि से ही कृषि है और ये आपस में अंतरंगता से जुड़े हुए है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत भूमि के रेगिस्तान में परिवर्तित होने के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए इसके निराकरण हेतु सम्पूर्ण विश्व को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाया गया। यद्यपि यह एक ज्वलंत समस्या है और इसका समाधान भी तत्काल आवश्यक भी है। किन्तु भूमि की गुणवत्ता में गिरावट केवल रेगिस्तान में परिवर्तित होने तक ही सीमित नहीं है, अपितु सम्पूर्ण विश्व में भूमि की गुणवत्ता में गिरावट अनेकों अन्य कारणों से भी तेजी से हो रही है, जिसके प्रति चिंता भी उतनी ही अनिवार्य है, जितनी कि जमीन के रेगिस्तान में परिवर्तित होने के कारण।
भारतवर्ष के अनेकों भागों में अत्यंत उपजाऊ भूमि, जिसमें जैविक कार्बन का प्रतिशत कभी 4 प्रतिशत या उससे भी अधिक रहता था, वह वर्तमान में आधा प्रतिशत या उससे कम हो गया है, जो कि उस मिट्टी की न केवल उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर रहा है, अपितु मिट्टी के अंतर्गत संचय हो सकने वाले कार्बन को कम कर रहा है, साथ ही मिट्टी में पनपने वाले सूक्ष्म जीव एवं अन्य जीवों तथा जैव विविधताओं को भी प्रभावित कर रहा है। इसी के साथ ही तेजी से बढ़ रही आबादी के कारण शहरों तथा गांवों की सीमाओं में हो रहा विस्तार, अधोसंरचना में भूमि के उपयोग, उद्योगों तथा खदानों में कृषि भूमि एवं उपजाऊ मिट्टी धारी भूमि वाले क्षेत्रों के उपयोग में परिवर्तन भी समानांतर रूप से चिंता का कारण होना चाहिए। यह एक ऐसा विषय है, जिसके प्रति केवल शासन तंत्र को जागरूक करने से समाधान नहीं हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस समस्त विश्व के अंतर्गत ज्यादातर देशों में एक शासकीय आयोजन के रूप में सीमित होता जा रहा है, जबकि इस दिन को पूरे विश्व के सभी नागरिकों के द्वारा उस विषय पर चिंता करने हेतु चिंतन किया जाना चाहिए और इसके समाधान के लिए प्रयास करने हेतु संकल्प किया जाना चाहिए, तभी विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन से कुछ सफलता संभव होगी।
वर्तमान में भूमि क्षरण के अलावे मौसम परिवर्तन के कारण कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव के सम्बन्ध में भी विश्वव्यापी चिंता बढ़ रही है। इसके अनेकों कारण हैं और उन कारणों का निदान करना कैसे संभव है, इस विषय पर चिंतन भी आवश्यक है। चूॅंकि सर्वाधिक दुष्प्रभाव भूमि पर विद्यमान कृषि तथा वानिकी एवं जैव विविधता पर अपेक्षित है, क्योंकि ये सभी पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित हैं। यद्यपि कृषि उत्पादकता पर मौसम परिवर्तन से होने वाले संभावित प्रभावों का विषय अन्य सभी प्रकार के संभावित प्रभावों में सबसे अधिक जटिल एवं पूर्वानुमान करने में कठिन विषय है।
मौसम परिवर्तन को पूर्णतः रोकना वर्तमान संस्कृति एवं सभ्यता एवं अर्थव्यवस्था के लिए लगभग असंभव सा ही है। चूॅंकि प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु एक आर्थिक मार्ग को ही वर्तमान पद्धति स्वीकृति प्रदान करती है एवं दुर्भाग्य यह है कि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु या पहले से उत्सर्जित कार्बन को भूमिगत करने हेतु या वनस्पतिगत करने हेतु जो लागत आती है, उस लागत की पूर्ति के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, उस धन के सृजन के प्रयासों से उत्पन्न होने वाले कार्बन की मात्रा ही दोगुना या तीन गुना हो जाती है। अतः केवल आर्थिक मार्ग से इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन तो क्या असंभव सा लगता है।
सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा का कार्बन फुटप्रिंट निर्धारित करें। अर्थात् एक इकाई मुद्रा के सृजन से कितने इकाई कार्बन डाईआॅक्साइड उत्सर्जन हो रहा है? उदाहरण के स्वरूप भारतवर्ष का जीडीपी वर्ष 2022-23 में 3.63 ट्रिलियन डालर है तो इस वर्ष में भारतवर्ष का सकल कार्बन उत्सर्जन 2.7 गीगा टन है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रति रूपए कार्बन इनटेंसिटी (कार्बन फुट प्रिंट).0.09 किलोग्राम है। अब प्रश्न यह उठता है कि, यदि हम मुद्रा के इस कार्बन इनटेंसिटी को कम करना चाहें तो वह कैसे होगा? और कैसे प्रत्येक रूपए में कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा? एक सरल समीकरण के रूप में 2022-23 में उत्सर्जन होने वाले इतने टन कार्बन को उत्सर्जन से रोककर भी यदि हमारी जीडीपी 3.63 ट्रिलियन डालर बनी रहती है, तब तो ऐसी अर्थव्यवस्था ही धारणीय अर्थव्यवस्था है, पर ऐसा करना कैसे संभव होगा? यही यक्ष प्रश्न है कि 2.7 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन को शून्य कैसे किया जावे? मौसम परिवर्तन एकाएक नहीं होता है और परिवर्तन की गति यदि अत्यंत धीमी होती है, तो प्रकृति की जो एडाप्शन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि पर दुष्प्रभाव काफी कम हो सकते हैं या प्रकृति स्वयं उन दुष्प्रभावों को सहने की शक्ति वनस्पति एवं जीवों में विकसित कर सकती है। चूॅंकि प्रकृति ने सदैव से जीव जगत को परिवर्तित हो रहे पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने की शक्ति प्रदान की है और इसी कारण से हम पाते हैं कि पृथ्वी में जो जैव विविधता है, उसमें -40 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले तापमान वाले ध्रुवों में भी जीवन है और रेगिस्तानी क्षेत्रों जहां 45-48 डिग्री सेल्सियस गरम तापमान होता है, वहां भी जीवन है। पर परिवर्तन यदि बहुत तेज होता है, जो कि साक्षात रूप से समक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से यह वनस्पति एवं प्राणी जगत के जीवन के लिए खतरनक ही सिद्ध होगा।
विश्व भर में यद्यपि मौसम परिवर्तन के प्रति चिंता प्रतिदिन अवश्य व्यक्त की जा रही है। किन्तु जब कभी भी इसके व्यावहारिक समाधान के लिए बात सामने आती है, तो ठोस पहल करने के लिए किसी में भी कोई तत्परता दिखाई नहीं पड़ती। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में जहां 145 करोड़ नागरिकों का वर्तमान एवं भविष्य निहित है, जो वर्तमान विश्व की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होता है। उस लोकतंत्र में किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा भारतवर्ष के कार्बन फुटप्रिंट को या भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्बन फुट प्रिंट को या भारतीय नागरिकों के कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के संकल्प को लेकर किसी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कोई उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका मुख्य कारण यह है कि इस वैश्विक समस्या के प्रति जन सामान्य को कोई गंभीर ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान नहीं है कि यह समस्या उनके दैनिक जीवन में बढ़ती मंहगाई या बेरोजगारी या पानी या बिजली या सड़क की समस्या से भी ज्यादा गंभीर है और इसका निवारण अन्य सभी स्थानीय समस्याओं के समाधान से भी ज्यादा जरूरी है।
लोकतंत्र की विवशता यही है कि जो बहुमत जन की अपेक्षा होगी, सरकार उसके अनुसार ही चलेगी। क्योंकि सरकार का चयन लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान और अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु ही किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पर्यावरण के समस्त पहलुओं के प्रति गहन जन जागरूकता लाकर ही हमें जन सामान्य की अपेक्षाओं की प्राथमिकताओं में प्रथम स्थान प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को प्रदान कराया जा सकता है। जन सामान्य को यह कदाचित पता नहीं है कि उनकी ज्यादातर दैनिक समस्याओं का स्रोत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके पर्यावरण तथा सघन प्रदूषण ही मुख्य कारण हैं। चाहे सूखे हुए कुएं हों या बोरिंग हों या नाले या तालाब में पानी की गंदगी है या ठोस अपशिष्ठों का अंबार या विषाक्त खाद्य इत्यादि। साथ ही इस पर्यावरणीय विनाश का स्रोत मानव मात्र है और उसकी बढ़ चुकी जनसंख्या, और बढ़ रही जनसंख्या सुरसा मुख की तरह इस पृथ्वी के पर्यावरण को तबाह कर रही है। तदैव यह गंभीर चिंता एवं विडम्बना का विषय है कि इस विशाल जन तंत्र में व्याप्त अधिकांशतः समस्याओं का मुख्य स्रोत जनसंख्या विस्फोट है। फिर भी इस पर कोई बहस क्यों नहीं है? जिसके कारण हरितकारी गैसों का उत्सर्जन तो बढ़ ही रहा है, वहीं भूमिगत जल एवं भूस्तरीय जल और कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में भी तेजी से गिरावट आ रही है। पर, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी अपने घोषणा पत्र में इसलिए नहीं रखा जाता, क्योंकि अनेकों धार्मिक आस्थाओं को मानने वाले लोगों को परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण को उनके धार्मिक आस्था के विपरीत बताया जाता है। जबकि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानव का कल्याण, प्रकृति का कल्याण एवं समस्त पृथ्वीवासियों के अंदर में आपसी सहृदयता और मधुरता ही है और होना चाहिए और दावा भी सभी धर्मों के प्रचारकों एवं प्रवर्तकों द्वारा यही किया जाता है। किन्तु जब व्यवहार में बातें आती हैं तो एक राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के फलस्वरूप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के उद्देश्य से आव्हान किया जाता है, जो कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक एवं धार्मिक आस्था के उद्देश्यों के भी अनुकूल शायद नहीं है। पृथ्वी पर व्याप्त इस सभ्यता ने अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमताओं से इस ब्रह्मांड के हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक के अंतरिक्ष को खंगाल लिया है। इस पृथ्वी को छोड़कर शेष ब्रह्मांड में अभी तक कहीं पर भी जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिला है। जीव सभ्यता या मानव सभ्यता मिलने की तो बात ही करना बेकार है। मेरी समझ में पृथ्वी पर जितने भी मनीषी किसी भी धर्म के नाम पर मानव को अपने व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु उपदेश किए हैं, उनमें कहीं पर भी ऐसा संदेश नहीं है कि मानव को मानव के प्रति राजसत्ता के लिए अर्थसत्ता के लिए या अन्य किसी भी प्रकार के लोभ एवं लालच के लिए हत्या और हिंसा या घृणा का आश्रय लिया जावे। धार्मिक उपदेशों का लक्ष्य एवं उद्देश्य प्रकृति एवं मानवता का कल्याण ही होना चाहिए।
मानव सभ्यता का अस्तित्व आज जब गंभीर संकट में है, तो इस संकट से मुक्ति के लिए धर्माचार्यों को वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे विवेचनाओं को आधार में लेकर अपने-अपने धर्मों के अंतर्गत ऐसे आचरणों को विज्ञान एवं तकनीकी के साथ संयुक्त करके अपने समाज को इस प्रकार से सशक्त करना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण आने वाली हजारों हजार पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य एवं सौहार्द्र बना रहे। किन्तु दुर्भाग्य यह है कि आज जो परिस्थिति पनप चुकी है, उससे तो ऐसा लगता है कि हमारे ही इस पीढ़ी को पृथ्वी पर प्रलय से साक्षातकार करना होगा। अभी तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसके अनुसार वर्ष 2024 में ही पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ चुका है, जबकि वैज्ञानिकों का ऐसा लक्ष्य था कि पृथ्वी पर कार्बन इमीशन को इस प्रकार से नियंत्रित किया जावे कि तापमान में यह वृद्धि वर्ष 2070 तक टाली जा सके और तब तक विज्ञान और तकनीकी में इतनी प्रगति को प्राप्त कर ली जावे कि कार्बन उत्सर्जन तब तक शून्य हो जावे।
बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते तापमान से आज दिल्ली जैसे राजधानी की दुर्गति यह हो गई है कि पीने के पानी के लिए लोग लम्बी-लम्बी कतारों में पानी का कनस्तर लिए पानी के टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं। सभी समाचारपत्रों एवं टेलीविजन मीडिया और तमाम तरह के प्रचार और संवाद माध्यमों में इसके लिए स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को दोषी ठहराने के लिए घंटों-घंटे बहस चलती है। किन्तु कोई भी समाचार चैनल, संवाद चैनल सामान्य नागरिकों के द्वारा किए जा रहे पर्यावरण विरूद्ध कृत्यों की विवेचना नहीं करते। किसी में भी साहस नहीं कि वह इस अव्यवस्था के लिए अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट को दोषी ठहरा सके। इस अव्यवस्था के लिए बेतहाशा नलकूप खनन को दोषी ठहरा सके। इस अव्यवस्था के लिए नागरिकों के द्वारा पानी के दुरूपयोग को दोषी ठहरा सके। पर्यावरण कानूनों के जंजाल भले कितने ही जटिल एवं दंडात्मक बना दिए जावें, पर क्या यह संभव है कि केवल पर्यावरणीय कानून के उल्लंघनों की सजा सुनाकर ही पर्यावरण को सुधारा जा सकता है? यह सभी के लिए विचारणीय विषय है और सभी को आपसी विचार-विमर्श एवं तालमेल से इस समस्या का समाधान जन जागृति और जन संकल्प से निकालना होगा, चूॅंकि पर्यावरण को बचाने के लिए सजा से ज्यादा सजगता जरूरी है। पत्रिका के सभी पाठकों को विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की शुभकामनाएं।