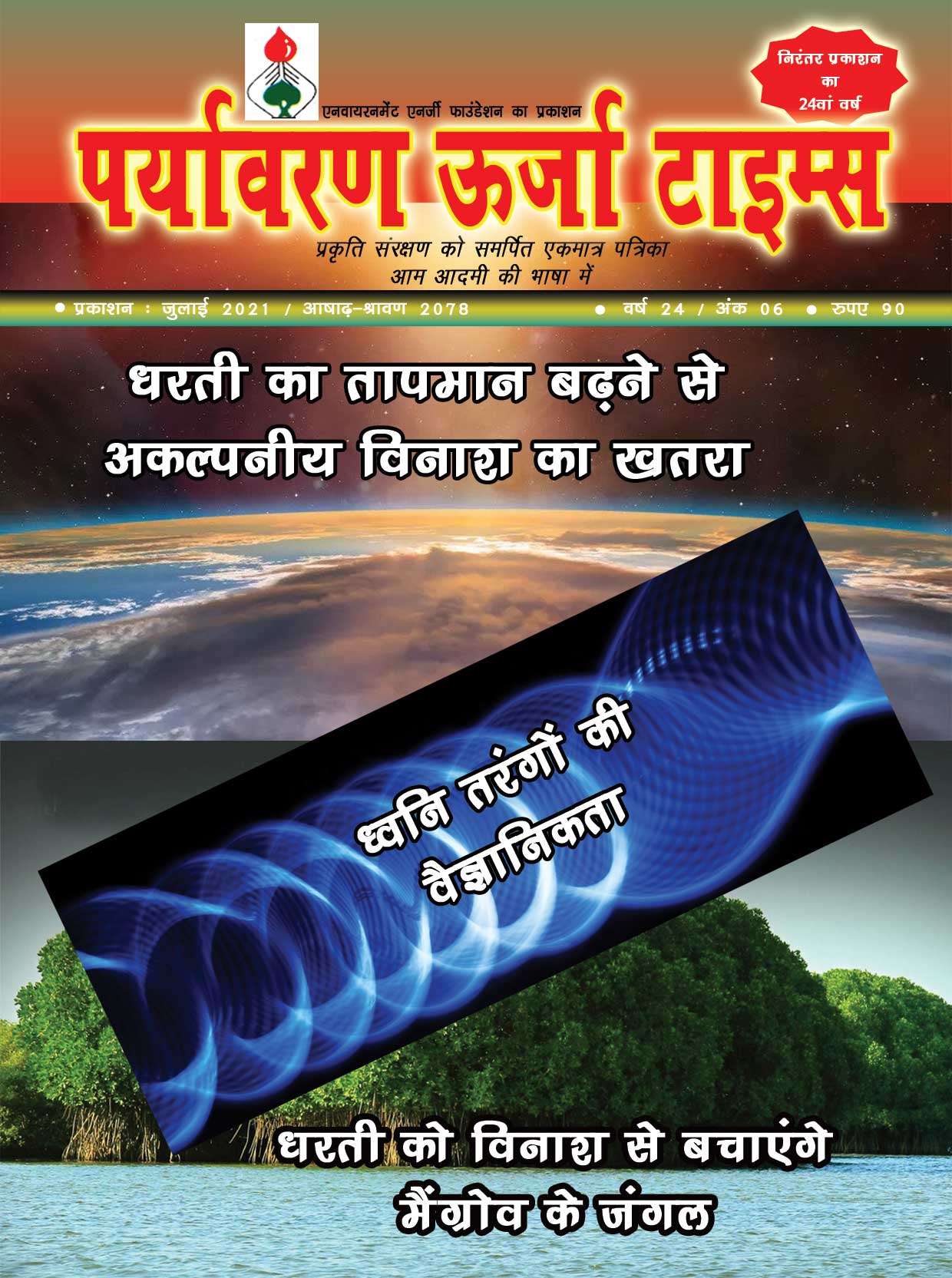संयुक्त राष्ट्र के मौसम परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन दिसम्बर 2019 में किया गया था, जिसकी आगामी बैठक नवम्बर 2020 में संभावित थी। किन्तु कोविड महामारी के दुष्प्रभाव के कारण इसे 21 अक्टूबर 2021 से 12 नवम्बर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लास्गो शहर के स्काटिक इवेंट चेम्बर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में मानवता को मौसम परिवर्तन के आसन्न संकट से मुक्ति दिलाने हेतु समस्त राष्ट्रों के द्वारा सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1994 में क्योटो प्रोटोकाल से आरंभ किए गए प्रयास से इस दिशा में अभी तक तय की गई दूरी काफी कुछ सकारात्मक एवं आशाजनक होती दिखती है। इसमें मुख्य रूप से सोलर पॉवर प्लांट, विंड पॉवर प्लांट से विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि तथा बहुत सारी औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता में वृद्धि निश्चित रूप से संज्ञान में लेकर साधुवाद एवं समर्थन के योग्य है। किन्तु, मौसम परिवर्तन के संकट को मानव सभ्यता से टालने के लिए अभी तक हुए प्रयास निश्चित रूप से पूर्णतया अपर्याप्त हैं। प्रतिवर्ष मौसम परिवर्तन के परिणामों की भयावहता एवं परिमाणों की विशालता स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अभी तक पिछले महीने में आई रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक में पिछले 30 वर्षों में 28 ट्रिलियन घनमीटर अर्थात 280 खरब टन के हिमखंड वाले ग्लेशियर से बर्फ लापता हो जाने का अनुभव है, जिसके दूरगामी परिणामों के असर खतरनाक हो सकते हैं।
सबसे बड़ा संकट यह है कि विश्व स्तर पर मौसम परिवर्तन के संकट को टालने हेतु आयोजित समस्त समझौतों को स्वीकार करना या न करना प्रत्येक देश की एक राजनैतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर है। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनी गई सरकारों की विविशता यह होती है कि राजनैतिक सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए लोक-लुभावने एवं तात्कालिक लाभ को प्रदर्शित कर अपने मतदाताओं से जन समर्थन प्राप्त कर सत्ता सिद्ध करें। इन परिस्थितियों में इन चुनी हुई सरकारों से यह अपेक्षा करना अत्यंत कठिन है कि तीव्र आर्थिक लाभ के एवं तीव्र आर्थिक प्रगति के जन आकर्षण से अपने आपको मुक्त कर आगामी पीढ़ी के लिए या दीर्घकाल के लिए कोई वर्तमान में कष्टदायक वैधानिक समाधान का सूत्रपात कर समाधान कर सकें।
इन परिस्थितियों में एक तरफ जब विश्व के समस्त न्यायविदों के द्वारा यह सर्वमान्य सिद्धांत लिया गया है कि ‘‘प्रदूषणकर्ता ही भार का भुगतान करे।’’ किन्तु, दूसरी ओर जब भी प्रदूषण के भार के आंकलन का प्रश्न उठता है तो सामान्य उपभोक्ता एवं पर्यावरण-प्रदूषण-भारजनक वस्तुओं के निर्माता उसके निर्माण में होने वाले भार को या उसके उपभोग में होने वाले पर्यावरण-प्रदूषण-भार को सम्यक रूप से आंकलन कर स्वीकार करने को तत्पर नहीं हैं। एक मोटे उदाहरण के तौर पर कोयले से बिजली बनाने पर एक इकाई बिजली को पैदा करने के लिए 0.8 किलो कोयला लगता है और इससे मान लीजिए आधा किलो कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन होता है। पर विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में निहित व्यक्ति केवल कोयले का मूल्य और उसके निर्माण की प्रक्रिया का मूल्य ही अपने ऊपर में भार मानता है। उसके विद्युत उत्पादन से उत्पन्न 0.5 किलोग्राम कार्बन डाईऑक्साइड और उसमें उपभोग में होने वाले एक लीटर पानी के खपत को वह निःशुल्क मानता है। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया में विद्युत उपभोक्ता भी सदैव विद्युत उत्पादक की तरह ही इन प्राकृतिक उपादानों के उपभोग का मूल्य कदाचित वहन नहीं करना चाहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों में प्रचलित कार्बन के घोषित दर को 15 डालर प्रति टन माने, या कि वर्तमान में भी चीन के द्वारा संपादित आंतरिक कार्बन बाजार में 8 डालर प्रति टन है, तो भी प्रति टन कार्बन का मूल्य 1000 रूपए बनता है। तद्नुसार लगभग 0.50 रूपए प्रति इकाई तो कार्बन उत्सर्जन टैक्स आज भी बनता है। जबकि वास्तव में तो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट (भंडार झ् अवरूद्ध) करने की लागत तो लगभग 25000 रूपए/टन आंकी जा रही है।
तदैव विडंबना यह है कि वर्तमान युग की भौतिक प्रगति का मूल्य भंगुर पर्यावरण को बलिदान कर आज भी जारी है। इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष या मूल कारण वर्तमान अर्थव्यवस्था समीकरणों में पर्यावरण क्षति के मूल्यांकन का कोई आंकलन, गणना में नहीं किया जाना है। अन्यथा भारत वर्ष में आज तक करोड़ों टन सड़ रहे जैव अपशिष्ठों से या तो बायो गैस में या बायो एथेनाल में परिवर्तन करना लाभदायक हो चुका होता।
वर्तमान परिदृश्य में कभी जब मैं अपने बचपन के दिनों को आज की प्रगति की तुलना में आंकलन करता हूॅं तो पाता हूॅं कि उस समय में जब मेरे गांव में किसी आदमी के हाथ में घड़ी नहीं होती थी, किसी के पैर में जूते नहीं होते थे, गांवों में बिजली नहीं थी, न तो पंखे थे और न वातानुकूलन यंत्र, न तो गैस के चूल्हे थे, न फोन था, न कार थी, न गाड़ियां थी, स्टेनलेस स्टील के बर्तन नहीं थे, टेलीविजन नहीं था, न मोबाइल था, पर 60 बरस पहले फिर भी हमारे गांवों में खुशहाली आज की तुलना में कहीं कम नहीं थी। यह सच है कि प्रगति के पथ से मानव सभ्यता को दैहिक सुख अवश्य मिला, पर प्रकृति को परास्त करते-करते मानव सभ्यता परास्त होने की तरफ बढ़ रही है।
मौसम परिवर्तन के भयावह दुष्परिणामों से संघर्ष करने वाले जन समूह शायद आज भी बिना बिजली के सूर्य के प्रकाश में जीवन-यापन के कष्ट को कम आंके-बनिस्बत अकाल मृत्यु के। पर विडंबना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन वंचितों की विडंबना को प्रस्तुत करने वालों की आवाज केवल एक एन.जी.ओ. की आवाज के रूप में नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह जाती है। तदैव आवश्यकता है, वैश्विक स्तर पर क्लायमेट समझौतों को नेगोशिएट करने का विधिक अधिकार सक्षम वैज्ञानिकों को एवं स्वयं सेवी संस्थानों को दिया जावे।
इस सत्य को स्वीकार किया जावे कि सम्पूर्ण विश्व का सर्वहारा जन, जहॉं एक तरफ सभी प्रकार के शासकीय कर (टैक्स) के भार को वहन करता है, तो वहीं सभी प्रकार के कार्पोरेट प्राफिट (वाणिज्यिक लाभ) का बोझ भी उसी के सर पर आता है, तो वहीं वर्तमान आधुनिक विकास जनित पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषण दुष्प्रभाव का भी सारा बोझ उसी पर आता है। अधारणीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से आम आदमी पर लादा जा रहा पर्यावरणीय दुष्प्रभाव का बोझ उसकी सहनशीलता की समस्त सीमाओं को लांघ रहा है। इसलिए जब सरकारें सुस्त पड़ रही हैं, तो प्रकृति ही शायद अपने पराक्रम से इस अधारणीय अर्थक्रम को परास्त करना चाहती है। समय की मांग तो यही है कि सम्पूर्ण अर्थ सिद्धांतों को पर्यावरणीय सिद्धांतों के सूत्रों से सन्निहित करके ही प्रगति का पथ नियोजित किया जावे।
– ललित कुमार सिंघानिया
समय की मांग तो यही है कि सम्पूर्ण अर्थ सिद्धांतों को पर्यावरणीय सिद्धांतों के सूत्रों से सन्निहित करके ही प्रगति का पथ नियोजित किया जावे