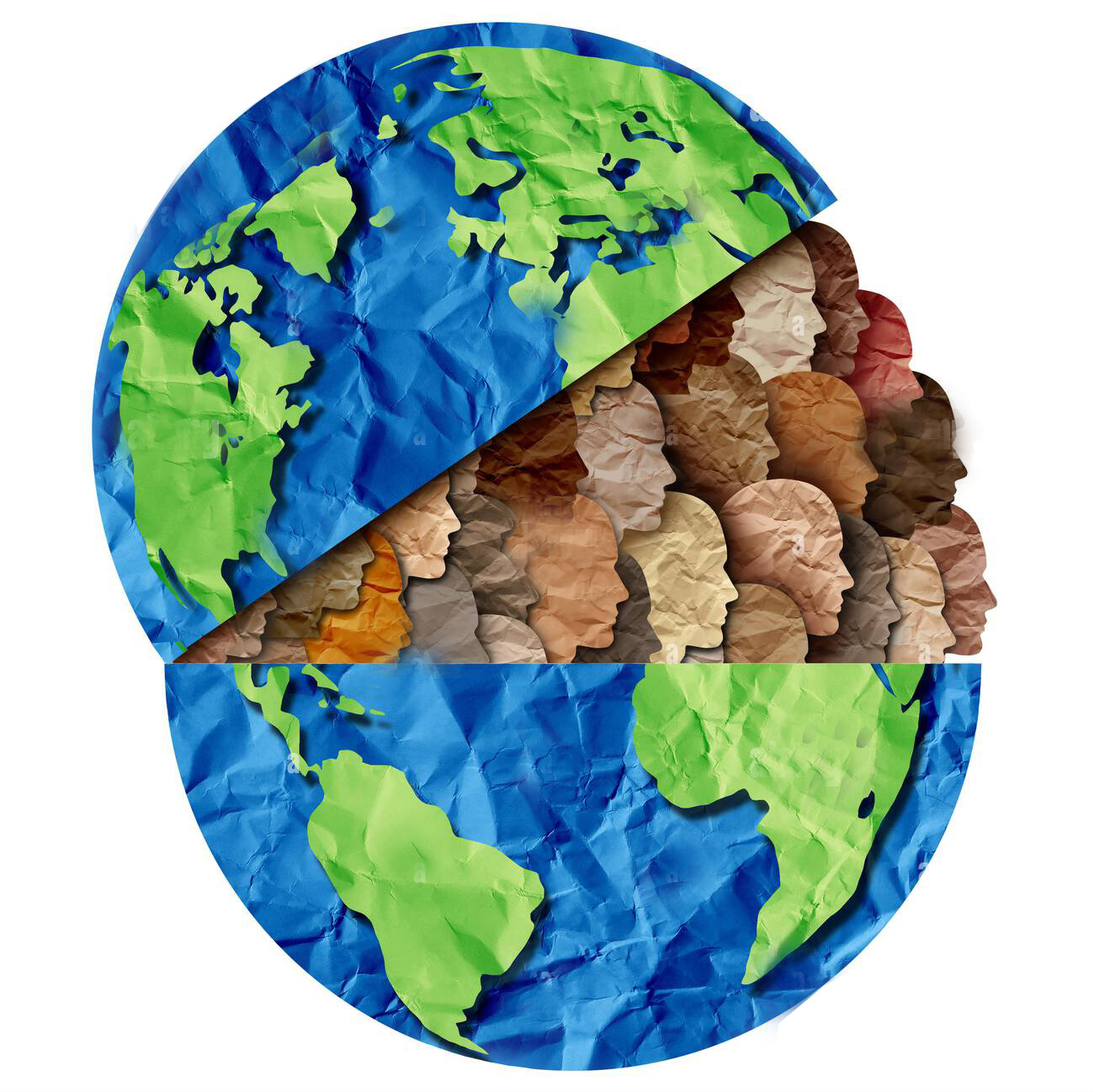आज के गंभीर पर्यावरणीय संकट के परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य विषय को लेकर जन-जन की चिंताओं को जानने, समझने तथा इसके उन अनछुए पहलुओं को समझाने के ऐतिहासिक लक्ष्य से विश्व जनसंख्या दिवस पर विश्व भर में जगह-अलग जन संगोष्ठी एवं सेमीनार आयोजित किए गए। यद्यपि पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत गंभीर और सर्वोच्च चिंता का विषय है, पर इस पर गंभीर चिंतन कर उसके मूल कारणों पर जाने तथा उसके समाधान पर चर्चा से ज्यादातर लोग कतराते हैं। कोई भी इस विषय पर सार्थक चिंतन तथा समाधानकारी कार्य करने के प्रति उतना गंभीर प्रतीत नहीं होता, जितनी गंभीर यह समस्या बन चुकी है।
जब भी प्रदूषण या पर्यावरण संकट की बात आती है, तो लोग सहजतापूर्वक सरकार को तथा सरकारी तंत्र पर दोष मढ़ देते हैं, या फिर उद्योग तथा कारखानों को ही दोषी मान लेते हैं। कुछ हद तक यह सही भी है, पर यह पूर्णतया सत्य भी नहीं है। क्योंकि इन सबके मूल स्रोत में यदि हम जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसका मुख्य कारण हमारी विस्फोटक हो चुकी जनसंख्या है और उसके साथ ही बदलते उपभोगवादी संस्कारों के कारण सुरसामुख की तरह हमारी पीढ़ी की अधिक से अधिक उपभोग करने की भूख है।
आज के समय की पुकार है कि किसी अन्य पर दोष चिन्हित करने से पूर्व हमें स्वयं की सोच तथा संस्कारों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें हमारे कृत्यों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का हिसाब लगाना चाहिए। हमें यह समझना अवश्य चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाॅं हैं, जिनके कारण हम अपने उपभोग को सीमित नहीं कर पाते? क्या हमारे संस्कारों में गिरावट है या और बातें?
यह बात जब पूरी दुनिया को ज्ञात है कि मानव तथा अन्य समस्त जीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों के पीछे मानव जनसंख्या ही है, तो फिर इस पर राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर बहस क्यों नहीं होती, कि कैसे इसे पूरी तरह से तत्काल नियंत्रित किया जावे? हमें यह अब खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि प्रकृति और परमपिता परमेश्वर ने जो हमें हमारी इस पृथ्वी पर प्राकृतिक सुरक्षित पर्यावरण तथा सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी संसाधनों को दिया है, उसे संभालने का सम्पूर्ण दायित्व हमारा ही है।
मानवीय संतानों को परमात्मा का प्रसाद या भेंट मानने वालों को यह चिंतन करना चाहिए कि, ईश्वर या परमात्मा द्वारा पृथ्वी पर हमें दिए गए भूभाग में वह स्वयं भी एक वर्गफुट की भी वृद्धि नहीं कर सकता, एक बूंद भी अतिरिक्त जल नहीं दे सकता और न ही अतिरिक्त अन्य कोई संसाधन ही दे सकता है। पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त संसाधन जो आज से कुछ लाख वर्षों पूर्व मानवों के लिए थे, उतने ही संसाधन आज के 815 करोड़ लोगों के समाज के लिए हैं।
वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों की रिपोर्टें हमें चीख-चीख कर बता रही हैं कि पृथ्वी माॅं की प्रकृति एवं पर्यावरण रूपी गोद में अब एक भी अतिरिक्त इंसान को संभालने के लायक जगह नहीं है। केवल जमीन ही सीमित नहीं है, अपितु शुद्ध तथा सुरक्षित जल भी सीमित है। कोयला, पेट्रोल तथा अन्य सभी खनिज भी सीमित हैं। आकाश में हरितकारी गैसों को संभालने का आयतन (स्पेस) भी अब खत्म हो चुका है। इन सबके बावजूद भी, यदि हम कुंभकर्णीय मुद्रा में सोते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे नाम को कोसेंगी। हमारी पीढ़ी को पर्यावरण तथा प्रकृति के विनाश करने वाले अपराधियों की संज्ञा देंगी। आज प्रकृति में प्रखर विकृति व्यापक है। पहाड़ों में वन नहीं हैं, वनों में वृक्ष नहीं हैं, पशु-पक्षी नहीं हैं, नदियों में शुद्ध जल नहीं है, आसमान में पारदर्शी स्पष्ट वायुमंडल नहीं है, मिट्टियों में उत्पादकता नहीं है, शुद्धता नहीं है, पर क्यों?
इसके पीछे और कोई नहीं, हम सब और विशेषकर मेरी यह पीढ़ी, जिसे हम लगभग 70 सालों से देख रहे हैं, वह जिम्मेदार है। हमने कभी भी इन सारी समस्याओं के मूल में मानवों की बढ़ती जनसंख्या को न स्वीकार किया है और न ही खुलकर इस पर बहस किया। अर्थशास्त्रियों ने हम मनुष्यों को केवल बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के उपभोक्ता के रूप में आर्थिक प्रगति का मोहरा बना दिया। किन्तु, कभी यह नहीं बताया कि मनुष्यों के इस बढ़ते उपभोग से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण या पर्यावरण क्षय के भरपाई की लागत, उस आर्थिक प्रगति के मूल्य से कई-कई गुना अधिक है।
अतः यह आत्मवलोकन अवश्य करना चाहिए कि सभी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, जातिगत संकीर्णताओं से मुक्त होकर मानसिकता शुद्ध करने का समय है। हमारी परमप्रिय पूज्य माॅं वसुंधरा (पृथ्वी) के पर्यावरण के आर्तनाद और चीत्कार के प्रति चिंता का समय है और यह निष्कर्ष लेकर संकल्प लेने का समय है कि इस मानव जनसंख्या को और अधिक विस्फोटक होने से कैसे रोका जावे? इस विशाल जनसंख्या के द्वारा बढ़ रहे संसाधनों के भोग को कैसे कम किया जावे? समाप्त हो रहे जंगलों, वनस्पतियों, पशु-पक्षियों को मानवीय जनसंख्या के प्रकोप से कैसे मुक्त रखा जावे?
इस चिंतन की गंभीरता को आपकी पीढ़ी के समक्ष रखने से पहले हमने यह समझने और जानने का प्रयास किया कि वर्तमान युवा पीढ़ी इस समस्या के संबंध में कितनी जानकारी रखती है तथा उन्हें इसकी गंभीरता का कितना आभास है? इस आयोजन के पूर्व अनेकों विद्यालयों में ‘पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स’ द्वारा इस विषय से संबंधित चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें लगभग 45 विद्यालयों से लगभग 2000 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इसमें लगभग 15 महाविद्यालयों से लगभग 200 छात्र-छात्राओं भाग लिया। हम इस अंक में इन प्रतिभागियों में से कुछ चयनित प्रतिभागियों के आलेख संक्षिप्त में प्रकाशित भी किए हैं।
पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स द्वारा 11 जुलाई को आयोजित जन संगोष्ठी में विद्वान वक्ताओं द्वारा अपने-अपने ढंग से प्रकृति और पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। डाॅ. रणजीत प्रसाद जो कि सेवानिवृत्ति विभागाध्यक्ष, धातुकर्म विभाग, एनआईटी जमशेदपुर से हैं, ने इसके वैज्ञानिक पक्ष को रखा। डाॅ. अनिल कुमार जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पर्यावरणीय विषय के प्रांतीय संयोजक एवं प्रचारक हैं, इस विषय के सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष को रखा। आचार्य महेश शर्मा जो कि संस्कृत एवं वेद विज्ञान के ज्ञाता हैं, वे पृथ्वी पर जनसंख्या और हमारे संस्कारों के भारतीय संस्कृति से संबंधित पक्ष को रखा।
बढ़ती जनसंख्या के बहुत सारे दुष्परिणामों का छात्रों ने अपने निबंध तथा वाद-प्रतिवाद एवं पोस्टर में अवश्य व्यक्त किया है, पर कुछेक आयाम अछूते हैं, जैसे कि जनसंख्या घनत्व दिल्ली में 20000 से अधिक लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के लिए मुश्किल से 50 वर्गमीटर स्थान है। न्यूयार्क में 11531 तो टोक्यो में 11025 तो वहीं मुॅंबई में 25550 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मनाली में 46000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत हैं। विश्व की जनसंख्या आज लगभग 812 करोड़ है, उसमें से भारत की 145 करोड़ है। अर्थात विश्व आबादी का 17.86 प्रतिशत लोग भारत में हैं जबकि भारत में पृथ्वी के कुल भूभाग का मात्र 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भाग ही है, जो कि पृथ्वी के 14.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का मात्र 2.21 प्रतिशत है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर को लगभग प्रजनन दर से अनुमानित किया जाता है, जो कि लगभग 2.139 है। पर यह प्रजनन दर विभिन्न समाजों में एक समान नहीं है। तदैव बहुधा ऐसा लगता है कि वास्तविक प्रजनन दर प्रकाशित आंकड़ों से कहीं बहुत ज्यादा है।
पर ऐसा मान भी लें कि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना सफल भी रहा तो विश्व की जनसंख्या 2086 तक 1043 करोड़ से 1100 करोड़ तक हो जाएगी। आज जहां विश्व में जनसंख्या घनत्व 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हे, वह 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा।
पर जब हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक जमाने में तो लोग अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा लड़के इसलिए पैरा करना चाहते थे कि उन्हें खेतों में काम करन के लिए लोग मिल सकें और इसके अलावे राजनैतिक उद्देश्य तो युद्ध लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की थी। और कुछ विश्वास यह भी था कि जिसका जितना बड़ा कुनबा, वह उतना ही समृद्ध और शक्तिशाली माना जाता था। पर कुछ धार्मिक विश्वास तो यह भी था और आज भी यही है कि संतान ऊपर वाले की देन है। तदैव जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतना अधिक उनके धार्मिक समाज का विस्तार होगा।
जबकि यह पूर्णतया भ्रामक और असत्य है। चूॅंकि यदि ऊपर वाला ही संतान देता होता, तो हरेक बच्चे के लिए कुछ जमीन भी अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) देता, कुछ खनिज और कुछ पानी भी अतिरिक्त रूप से ज्यादा देता और बिना विवाह के भी संतान देता। किन्तु हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। यह एक भ्रामक और घातक चिंतन है, जो किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण तथा प्रकृति के प्रतिकूल ही है। किसी भी प्रकार से विज्ञान सम्मत नहीं है।
पर, आज के इस अर्थप्रधान युग में मानव संख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने का विचार अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रसारित किया जाता है। चूॅंकि प्रत्येक नया मनुष्य बाजार का एक नया उपभोक्ता है, चाहे किसी अन्य वस्तु का उपभोक्ता हो या न हो, पर पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सीमित जीवन के लिए अनिवार्य संसाधनों जैसे शुद्ध जल, आवास, ऊर्जा, भोजन आदि का क्रेता तो अवश्य है। चूॅंकि इन सभी प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपादानों पर भी आज आर्थिक बाजार का कब्जा हो चुका है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक नए नागरिक के जन्म से इनके उपभोग में वृद्धि होती है और बाजार का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त ‘‘अर्थशास्त्री’’ मनुष्यों को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में भी अनिवार्य घटक मानते हैं।
किन्तु, अर्थ की परिभाषा में भले ही जनसंख्या मानव श्रम जनित उत्पादकता एवं सेवा अर्थ (धन) के आकार को विस्तार देते हैं, किन्तु प्रश्न यह उठता है कि प्रत्येक अतिरिक्त मनुष्य क्या प्रकृति एवं पर्यावरण के शोषण के बिना भी कुछ पैदा कर सकता है? यदि नहीं, तो अगला प्रश्न यह निश्चित रूप से उठता है कि पर्यावरण तथा प्रकृति के उपभोग से उत्पन्न क्षति की पूर्ति की लागत क्या है और उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या है?
इस गणना से हम पाते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक रूप से भी घाटे का सौदा है। इस युग में मनुष्य की संख्या में वृद्धि का कारण कुछ हद तक तकनीकी तथा ऊर्जा एवं संचार की क्षमताओं में विस्तार के कारण भी है। यह सच है कि विद्युत ऊर्जा एवं इंटरनेट संचार ने जीवन को सुखद एवं गतिशील बना दिया, पर यह गंभीर चिंता का विषय है कि यदि कभी एकाएक किसी भी कारण से विश्व से विद्युत ऊर्जाउत्पादन संयंत्र ठप्प हो जाएं या इंटरनेट सेवाएं ठप्प हो जाएं, तो क्या गंभीर हादसा होगा?
मानव सभ्यता इन कृत्रिम साधनों के बिना भी सुखद संसार में हजारों वर्षों से जीती आई है। आज भी मनुष्य के अलावे अन्य सभी जीव-जंतु, वनस्पति बिना किसी कृत्रिम साधनों या तकनीकी आश्रय के सुखपूर्वक जीते हैं। पर इन साधनों के आविर्भाव से मनुष्यों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसके प्रतिमूल प्रभावों का खामियाजा मनुष्यों के अलावे अन्य जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों को झेलना पड़ा है और पड़ रहा है।
आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट लगातार धरती के तापमान का बढ़ना है, जलवायु परिवर्तन होना है। इसके दुष्परिणाम आज हमारे समक्ष हैं। दिल्ली में एक दिन में 9 इंच पानी का बरसना या मक्का में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का पहुॅंचना, ग्लेशियरों का पिघल जाना, ध्रुवीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल का घटना आदि संकट भविष्य के नहीं, अपितु वर्तमान में साक्षात हैं। अब इन परिस्थितियों में लड़ाई को कल के लिए टाला नहीं जा सकता है। यदि इससे लड़ना है तो हमारे संकल्पों में सबसे गंभीर संकल्प जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण विराम ही लगाना होगा।
इसके लिए जन चेतना एवं जन जागृति जरूरी है। इस चेतना में यह समझना और समझाना जरूरी है कि पृथ्वी पर बढ़ रही मानव जनसंख्या परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक है और यह विस्फोट की कगार में पहुॅंच चुकी है। यदि इसे रोका नहीं गया, तो हमारी पृथ्वी पर समस्त जीवों को लुप्त होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उन जीवों में मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।
साथ ही यह भी खुलासा जरूरी है कि किसी भी देश में या सारी दुनिया में चाहे 100 प्रतिशत लोग किसी भी धर्म विशेष को ही क्यों न मानने लगें, चाहे
सभी धरतीवासी केवल एक ही धर्म और एक ही जाति या एक ही भाषा-भाषी ही क्यों न हो जावें, तब भी पृथ्वी पर यदि मानव संख्या 1000 करोड़ पार कर गई तो शायद किसी का भी सुरक्षित बचना संभव नहीं होगा।
यदि हम अपनी पहल से इस विपदा को आने से नहीं रोकेंगे, तो कुदरत अपनी लाठी से हमें समाप्त कर देगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम सब जागें और जगायें। जन-जागृति लाएं और यदि आवश्यक हुआ तो सभी देशों की सरकारों पर, संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनायें कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर जनसंख्या वृद्धि को शून्य किया जावे। इस बात का भी स्पष्ट खुलासा जरूरी है कि कोई भी संतान ऊपर वाले की देन नहीं है। यह हमारे मानवीय संसर्गों की ही परिणिति है। इसमें ऊपर वाले की कोई भूमिका नहीं है।
हमारी पृथ्वी पर लैंड स्पेस सीमित है, वाटर स्पेस सीमित है, एनर्जी स्पेस सीमित है, खनिज साधन स्पेस सीमित हैं और सबसे ज्यादा सीमित है कार्बन स्पेस। आई.पी.सी.सी. के द्वारा वर्ष 2023 अक्टूबर में किए गए अनुमान के अनुसार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए 500 बिलियन टन तक ही अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को रोकना होगा। चूंकि, वर्ष 2019 तक ही लगभग 2516 बिलियन टन कार्बन वातावरण में डाला जा चुका है। पर अनेकों वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पास मात्र 100 बिलियन टन ही कार्बन उत्सर्जन का स्पेस है।
जबकि वर्ष 2023 में ही लगभग 37.55 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन किया गया है। तदैव यदि यही दर कायम रही तो आगामी 3 साल में ही 100 बिलियन टन स्पेस खत्म हो जावेगा। अन्यथा आगामी 14 वर्षों में तो 500 बिलियन टन स्पेस भी खत्म हो जावेगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि हमने आज इसी जनसंख्या के जीवन यापन के लिए पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा संभाल सकने वाली कार्बन आयतन की संपूर्ण क्षमता को भोग कर समाप्त कर दिया है।
कड़वा सच तो यह है कि हमने एक दियासलाई (माचिस की तीली) को जलाने से उत्पन्न कार्बन को संभालने के लिए भी जगह शेष नहीं छोड़ा है। पर विस्फोटक हो रही जनसंख्या के द्वारा कार्बन उत्सर्जन खतरनाक स्तर पर बदस्तूर जारी है।
आज भारत में प्रति व्यक्ति औसतन 2.00 टन प्रतिवर्ष (विश्व का 7ः) कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है। जबकि 80 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। वहीं विश्व के कुछ समृद्ध देशों में अमेरिका के नागरिकों द्वारा 14.44 टन/वर्ष (विश्व का 12.66ः), तो चीन के नागरिकों के द्वारा 8.85 टन/वर्ष (विश्व का 32.88ः) कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा हैं
हम यह देख रहे हैं कि बढ़ती समृद्धि के कारण भारत में और अन्य देशों में भी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती समृद्धि क्या हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध नहीं होगी? चूॅंकि, समृद्धि की चाहत सबकी है, तो कम से कम जनसंख्या को ही नियंत्रित करने का प्रयास क्यों न करें?
हमें यह चिंता करना आवश्यक है कि यदि जनसंख्या यूं ही बढ़ती रही और भारत की आर्थिक प्रगति की दर भी यूॅं ही कायम रही, तो हम कैसे हमारे कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे? जैसा कि अनुमान है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि प्रति वर्ष 0.30 प्रतिशत भी रही तो वर्ष 2050 तक यह 145 करोड़ से बढ़कर 167 करोड़ हो जावेगी। इस जनसंख्या वृद्धि के साथ ही यदि हम सतत आर्थिक वृद्धि को भी वर्तमान दर से ज ारी रहने का अनुमान करते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वर्तमान 2.00 टन/वर्ष कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
चूॅंकि, हम विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन का स्तर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि फ्रांस में 4.76 टन, इटली में 5.48 टन, पोलैंड में 8.5 टन, वियतनाम में 3.27 टन, यहां तक कि ब्राजील में 2.15 टन और मेक्सिको में 3.56 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है।
ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी अर्थव्यवस्था देश के वर्तमान 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए विकास के जो भी कार्य करने का संकल्प लेती है, उन सभी कार्यों के कारण ऊर्जा की मांग में वृद्धि स्वाभाविक है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोई भी कार्बन उदासीन (कार्बन न्यूट्रल) स्रोत निकट भविष्य में दिखाई नहीं देते। जिन स्रोतों से कार्बन उदासीन ऊर्जा संभव है, उसमें सोलर तथा पवन ऊर्जा के लिए अब अतिरिक्त भूभाग को कृषि से बाहर करना भी अन्न संकट पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास, अधोसंरचना, अनाज, फल, सब्जी, पानी इत्यादि हेतु बए़ती जमीन की व्यवस्था करना भी दूभर है। अतः यह सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है कि हम तत्काल सम्पूर्ण जनसंख्या नियंत्रण करें।
ऐसी विषम परिस्थितियों का वैज्ञानिक ज्ञान आज की वर्तमान पीढ़ी के कितने लोगों में है? क्या आप में से किसी को पता है कि यदि यूॅं ही प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाते रहे और यूॅं ही पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि को अनियंत्रित करते रहे तो पृथ्पी पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि कब हो जावेगी? यदि पृथ्वी पर 1.5 डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि हो जावेगी, तो दोनों ध्रुवों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर कितना बढ़ जावेगा? यदि जल स्तर इतना बढ़ गया तो पृथ्वी का कितना बड़ा भूभाग समुद्र में समा जावेगा? कितनी उत्पादकता में कमी आवेगी और इसके क्या दुष्परिणाम होंगे?
विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को भले ही इस कड़वे सच का ज्ञान हो, पर मुझे लगता हे कि इस खतरनाक सच को वे अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तभी तो 28 से अधिक बार कांफ्रेस आफ पार्टीज की बैठकों के बाद भी किसी भी बैठक में बढ़ती जनसंख्या को इस दुर्दशा का जिम्मेदार नहीं माना है। इसलिए कोई भी देश इसके समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करता है। इस खतरनाक भूल को सुधारने की दिशा में युवा जन-जागृति आवश्यक है। अब आपकी युवा पीढ़ी ही फैसला ले कि हमें क्या करना चाहिए?
हमें संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव बनाना चाहिए कि अगले ब्व्च्29 में जनसंख्या विस्फोट का प्रकृति एवं पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभाव पर खुली चर्चा करें एवं सम्पूर्ण जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रस्ताव पारित करें। इसके साथ ही इस विषय पर समस्त जानकारियाॅं भारतीय राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रकाशित करें। भारत सरकार को कहा जावे कि जनसंख्या विस्फोट के प्रकृति और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जावे। अर्थशास्त्रियों को निर्देश दिया जावे कि अधारणीय विकास से जनित पर्यावरण दुष्प्रभाव का मूल्यांकन कर जीडीपी के साथ ही ग्लोबल एनवायरमेंटल डैमेज कास्ट को प्रकाशित किया जावे। विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि से पनप रहे पर्यावरण विनाशकारी संस्कारों पर अंकुलश लगाने कानून बनाया जावे, चाहे वे कार्य धार्मिक हों, सामाजिक हों, राजनैतिक हों या प्रशासनिक हों। सभी देशों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु तत्काल कानून बनाने की मांग की जावे।
स पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स